
मुजफ्फरपुर / गया / पटना / नई दिल्ली : देश को अभी आज़ादी भी नहीं मिली थी। मध्य बिहार के गया जिले में साल 1928 में जन्म लिए ललित मोहन शर्मा पटना विश्वविद्यालय से 1946 में स्नातक और फिर 1948 में विधि में स्नातक करने के बाद 1949 में पटना उच्च न्यायालय में आर्टिकल्ड क्लर्क के रूप में नामांकित हुए और फिर 1950 के प्रारंभिक वर्षों से उच्च न्यायलय में एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास शुरू किये। सात साल बाद 1957 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। देश आज़ाद हो गया था, साथ ही, देश को एक गणराज्य घोषित हुए सात वर्ष हो गए थे। शर्मा जी अपनी लगन, मेहनत के बल पर सर्वोच्च न्यायलय के वरिष्ठ अधिवक्ता नामित हुए। पंद्रह वर्ष बाद साल 1973 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किये और फिर साल 1987 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किये। सर्वोच्च न्यायालय में पांच वर्ष बाद न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा को 18 नवंबर 1992 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर.नारायणन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाये। यह भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए गर्व की बात थी।
न्यायमूर्ति शर्मा से पूर्व, कल के शाहाबाद और आज के भोजपुर जिले के न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा पटना विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक और 1921 में स्नातकोत्तर करने के बाद 1922 से 1927 तक पटना उच्च न्यायालय में वकालत किये। बाद में, विधि महाविद्यालय में प्राध्यापक भी बने। समयांतराल अपने ही विश्वविद्यालय के विधि संकाय की सीनेट और विधि परीक्षा बोर्ड के सदस्य भी बने। साल 1940 आते-आते सरकारी अधिवक्ता और फिर पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे। आज़ादी के महज चार साल बाद पहले नागपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और फिर 1954 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायमूर्ति के पद पर आसीन हुए। जब देश 12 वां जश्ने आज़ादी मना रहा था, उसके दो माह बाद, न्यायमूर्ति सिन्हा (राजपूत) न केवल अपने प्रदेश, अपना न्यायालय (पटना उच्च न्यायालय), बल्कि अपने समाज का नाम रौशन कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के छठे सम्मानित मुख्य न्यायाधीश के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा शपथ लिए।
साल 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर अपने नये अस्तित्व में आया था। इसके चार साल बाद 3 फरवरी, 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। 28 जनवरी 1950 को, भारत के एक प्रभुतासंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ, जहाँ 1937 से 1950 तक, भारत संघ न्यायालय 12 वर्षों के लिए कार्यरत था। भारत का उच्चतम न्यायालय 1958 में तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। अब विचार कीजिए – पिछले 76 वर्षों में बिहार के पटना उच्च न्यायालय से अब तक सिर्फ दो न्यायमूर्ति देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ पाए हैं। एक: न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा (राजपूत – अक्टूबर, 1959 से 31 जनवरी, 1964 तक) और दो: न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा (भूमिहार – 18 नवम्बर, 1992 से 11 फरवरी, 1993 तक) – यह बिहार के लिए गर्व की बात है।

चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अब तक 51 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं और बिहार में विगत 2022 जाति- आधारित जनगणना के आधार पर प्रदेश में 214 जातियां हैं, जिसमें 22 जातियां – अनुसूचित जाति, 32 जातियां – अनुसूचित जनजाति, 30 जातियां – पिछड़ी जाति, 113 जातियां – अत्यंत पिछड़ी जाति और 7 जातियां – ऊँची जाति घोषित किये गए । इन आंकड़ों को यहाँ इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि बिहार के वर्त्तमान (2024) जनगणना के आधार पर प्रदेश की कुल आवादी 132,790, 000 में से अब तक एक कायस्थ और एक भूमिहार को छोड़कर, दिल्ली सल्तनत में आईटीओ चौराहे से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से अंकित तिलक मार्ग और दिल्ली से कृष्ण की नगरी मथुरा की ओर जाने वाली सड़क मथुरा रोड के बीच स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सम्मानित मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुँचने वाले इन दो जातियों – कायस्थ और भूमिहार के अलावे – कोई नहीं हैं? यह भी शर्म की बात है।
क्योंकि प्रदेश में कुकुरमुत्तों की तरह नेता, ठेकेदार, बिचौलिए तो उत्पन्न हो रहे हैं अपने-अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, ऐसी स्थिति में कल तक जो गरिमा का प्रतीक थे, आज इन नेताओं के सामने ठेंघुने- घुटने के बल खड़े रहकर अपनी गरिमामय अतीत को ना ही सुरक्षित रख पा रहे हैं और ना ही इसमें इजाफा करने में सफल हो रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो उस क्षेत्र में विख्यात नहीं, ‘तथाकथित रूप से कुख्यात’ हो रहे हैं, अपने समाज और पूर्वजों के सम्मान में इजाफा नहीं कर पा रहे हैं, यह भी दुखद है। शब्द बहुत कटु है, लेकिन शायद सत्य यही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था में बिहार का, खासकर भूमिहारों, कायस्थों और ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा, अथवा है, एक गहन शोध का विषय है। लेकिन अगर प्रदेश में सातवाँ, आठवाँ, कक्षा पास, मैट्रिक अनुत्तीर्ण, अविचारवान, अकुशल, अयोग्य व्यक्ति राजनीतिक गलियारे में कुर्सी तोड़ेंगे, तो आप ऐसे शोध के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज 77 वर्ष गणतंत्र के बाद अगर प्रदेश की साक्षरता दर महिला-पुरुषों में 77 फ़ीसदी भी नहीं हो पाया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है।
चलिए बिहार के कुछ ऐसे हस्ताक्षरों के बारे में चर्चा करते हैं जो सात उच्च जाति की श्रेणी में हैं (उन दिनों राजनीतिक लाभ के लिए जातीय जनगणना होने की बात नहीं थी) भूमिहार, कायस्थ, राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोग अव्वल थे। शुरुआत न्यायमूर्ति एन.पी. सिंह से करते हैं। सिंह 1956 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए और अप्रैल 1973 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। साल 1991 में पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने और फिर फरवरी 1992 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाले। चार माह बाद जून 1992 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति नागेंद्र राय साल 1966 में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए थे। वे मुख्य रूप से पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक, सिविल और संवैधानिक मामलों में अभ्यास किये थे। साल 1990 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 2005 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने।
न्यायमूर्ति नारायण रॉय साल 1972 में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। उन्होंने मुख्य रूप से पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक, सिविल और संवैधानिक मामलों में अभ्यास किये। साल 1986 में पटना उच्च न्यायालय की रांची पीठ में सरकारी अधिवक्ता बने।वर्ष 1991 में पटना उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने और अक्टूबर 2007 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। वह झारखंड के गिरिडीह जिले के एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

डॉ. कृष्ण नंदन सिंह पटना उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। वे दून स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने मुख्य रूप से पटना और रांची उच्च न्यायालयों में संवैधानिक, प्रशासनिक, कॉर्पोरेट, आपराधिक और मध्यस्थता मामलों में महारत प्राप्त किये। शिवहर राज के डॉ. के.एन. सिंह का नाम उद्धृत किया जा सकता है। उसी तरह, आर.वी.शाही, भारत के पूर्व ऊर्जा सचिव जो एनटीपीसी के निदेशक और बीएसईएस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।प्रख्यात चार्टर्ड एकाउंटेंट एस.के.शाही, पी.के. शाही वर्तमान में बिहार सरकार के महाधिवक्ता हैं, भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह का नाम कैसे छोड़ जा सकता है।
बाबू दिग्विजय नारायण सिंह के पुत्र डॉ. प्रगति सिन्हा कहते हैं: भूमिहार, राजपूत और कायस्थ समाज के लोगों ने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाओं में अपनी पहचान अद्भुत बनाये – इस बात को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन सत्तर के दशक के प्रारंभिक वर्षों से इस समाज के साथ साथ बिहार के सभी ऊँची जाति के लोगों में ऐसी कौन सी अवधारणा का विकास हो गया जिससे एक तो यह समाज ‘व्यवस्था’ से ‘भयभीत’ होने लगा, उनकी गरिमा पर आँच आना शुरू हुआ, और वे व्यवस्था से टकराने की हिम्मत छोड़ कर मूक-बधिर हो गए। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि वे अपने समाज और तत्कालीन हस्ताक्षरों की गरिमा को रेल की पटरियों की तरह अलग-थलग कर जीवन का मार्ग बदल दिये। तभी तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद बिहार में यह समाज, पहले जहाँ हुंकार भरने की कूबत रखता था, हुंकार से भयभीत होने लगा।
डॉ. प्रगति सिन्हा का कहना है कि “आज जो स्थिति देखता हूँ उसे देखकर कतई विश्वास नहीं होता। चतुर्दिक गिरावट है। पढ़ने-लिखने की बात तनिक देर के लिए छोड़ भी दें, तो आज भूमिहार ब्राह्मण के लोग रंगदारी से राजनीति तक, सिनेमा हॉल के मालिक से बसों, ट्रकों के परिवहन व्यवसाय में प्रवेश कर लिए हैं। कल इस समाज को जहाँ कलम-दवात की ताकत से आँका जाता था, आज आंकने का यंत्र भी बदल गया है। आज सभी एक दूसरे के पेअर खींचने में लगे हैं। निजी स्वार्थ के लिए राजनीती होती है। सामाजिक सरोकार से अब (अपवाद छोड़कर) लोगों को दूर-दूर तक कोई नाता-रिश्ता नहीं रह गया है। यह इस समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है, जहाँ तक अगली पीढ़ी का सवाल है।” वैसे यह भी एक गहन शोध का विषय है क्योंकि गिरावट लालू यादव के कालखंड से प्रारब्ध हुआ ।
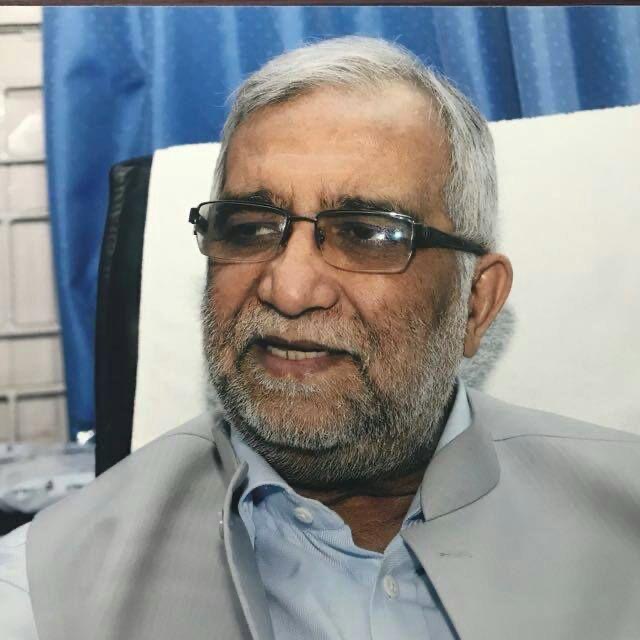
चिकित्सा सेवा में बिहार के भूमिहारों का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। डॉ शीतल प्रसाद सिंह जिनका नाम प्रदेश के मेडिकल सोसायटी में सबसे अधिक सम्मान से लिया जाता है। प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सकों में डॉ विजय नारायण सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के शल्य चिकित्सा विभाग के सबसे लंबे समय तक विभागाध्यक्ष रहे और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पटना में कृष्णकांत बाबू के साथ एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया, जिसे नालंदा मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसी तरह डॉ ए के एन सिन्हा जो भारतीय चिकित्सा संघ में सबसे बड़े व्यक्ति और कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ-साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के सबसे लंबे समय तक सेवारत अध्यक्ष रहे। डॉ. सिन्हा एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ भी थे।
पश्चिम पटना के पैथोलॉजिस्ट डॉ जी पी शर्मा जिन्होंने डॉ जी पी शर्मा लैब की शुरुआत की। 1948 में पीएमसीएच से एमबीबीएस की डिग्री पास की और रेडियोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए लंदन गए और पीएमसीएच में रेडियोलॉजी के आजीवन विभागाध्यक्ष बने डॉ जे पी सिन्हा। डॉ. सिन्हा 1980 में प्रतिष्ठित पीएमसीएच के प्रिंसिपल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनके पोते भी वर्तमान में लन्दन में रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉ सिन्हा भगवानपुर-रत्ती, लालगंज, वैशाली के मूल निवासी हैं।
इसी तरह डॉ आर के सिंह और डॉ अमित कुमार डॉ राज किशोरी सिंह प्रसूति एवं स्त्री रोग में विशेषज्ञता वाली बिहार की सबसे प्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक हैं। उनके बेटे डॉ अमित कुमार भी बिहार में एक प्रसिद्ध बांझपन विशेषज्ञ हैं। डॉ यू एन शाही। डॉ धन पति राय जिन्होंने 1939 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की और समाज की सेवा करने के लिए अपने पैतृक स्थान पर बस गए। उनके पुत्र डॉ बी बी राय भी 1962 के डीएमसीएच के पूर्व छात्र हैं और एचईसी रांची में आर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर चुके हैं। डॉ बी बी राय के पुत्र श्री संजीव कुमार रॉय सिंगापुर में बसे हुए हैं और एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय श्रेणी प्रबंधक की क्षमता में एक एमएनसी का नेतृत्व कर रहे हैं। जबकि उनके दूसरे पुत्र श्री राजीव कुमार राय एक सिविल सेवक थे, लेकिन अब कनाडा में बस गए हैं।

डॉ बी पी मिश्रा मुजफ्फरपुर में एस के मेडिकल कॉलेज के पहले प्राचार्य बने। डॉ. बी पी मिश्रा मुजफ्फरपुर में मॉडर्न डायग्नोस्टिक लैब नाम से अपनी पैथोलॉजी क्लिनिक चलाते हैं। उनके बेटे डॉ. रंजन मिश्रा भी पैथोलॉजी विशेषज्ञ हैं, जबकि उनके भतीजे डॉ. के के मिश्रा ने मनियारी महंत की पोती डॉ. रंजना मिश्रा से विवाह किया है और वे अपना पैथोलॉजी क्लिनिक स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक लैब चलाते हैं। डॉ. के के सिन्हा रांची के एक न्यूरोसर्जन, पूर्वी भारत, विशेष रूप से झारखंड और बिहार के चिकित्सा पेशे में प्रमुख हस्तियों में से एक हैं। डॉ. अनमोला सिन्हा एक दुर्लभ चिकित्सक। डॉ एन के एन सिन्हा, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से मेडिसिन के सेवानिवृत्त प्रोफेसर उद्धृत किया जा सकता है। वे रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन (एफआरसीपी) के फेलो हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं।
डॉ राजेश्वर ठाकुर एक प्रसिद्ध सर्जन होने के साथ-साथ एक उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षक भी हैं। वे कमरगामा, कल्याणपुर, समस्तीपुर के मूल निवासी हैं। चिकित्सा शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद वे सर गणेश दत्त सेवा संस्थान, पीएमसीएच ओल्ड बॉयज एसोसिएशन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉ आर बी शर्मा और डॉ उषा शर्मा न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध सर्जन हैं और उन्होंने लंदन और अमेरिका में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। डॉ शांति रॉय और डॉ अनीता सिंह बिहार की सबसे प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति एवं स्त्री रोग डॉक्टरों में से एक हैं। उनके बेटे डॉ हिमांशु राय भी बिहार के जाने-माने बांझपन विशेषज्ञ हैं। डॉ शांति रॉय की छोटी बहन डॉ अनीता सिंह भी एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जो पटना मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिहार में कार्डियोलॉजी में दूसरे डीएम हैं।
पद्मश्री डॉ. चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जिन्हें आमतौर पर डॉ. सी. पी. ठाकुर कहा जाता है, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के मेडिसिन के एमेरिटस प्रोफेसर हैं, उन्हें कालाजार के उपचार में दवा की प्रतिक्रिया को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा चिकित्सा विज्ञान (क्लीनिकल रिसर्च) के क्षेत्र में रैनबैक्सी रिसर्च अवार्ड्स भी मिल चुका है। उनका नया ज्ञान जल्द ही कालाजार, विसराल लीशमैनियासिस के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा से एक दवा विकसित करने की दिशा में ले जा सकता है। वह स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और पटना निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार लोकसभा के सदस्य हैं।
प्रबंधन गुरु पद्मश्री डॉ. प्रीतम सिंह सिंह जिन्होंने अपना जीवन भारत और विदेशों में प्रबंधन शिक्षा के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने आईआईएम लखनऊ और एमडीआई के लिए दुनिया भर में सहयोग विकसित किया और अमेरिकी, यूरोपीय, कनाडाई, ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई प्रबंधन स्कूलों के साथ छत्तीस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में बौद्धिक पूंजी के निर्माण और आईआईएम बैंगलोर को वास्तव में एकीकृत प्रबंधन स्कूल के रूप में फिर से केंद्रित करने में उनके योगदान के कारण उन्हें एक उत्कृष्ट परिवर्तन गुरु और पुनर्जागरण नेता के रूप में जाना जाता है। एमडीआई के निदेशक के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान एमडीआई के नाटकीय बदलाव और आईआईएम लखनऊ को आईआईएम एल के निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नंबर 1 संस्थान के रूप में फिर से स्थापित करने के कारण उन्हें जादुई निदेशक की प्रतिष्ठा मिली। देश के लगभग सौ संस्थानों के बोर्ड सदस्य के रूप में उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में परिवर्तन प्रक्रिया को सक्रिय रूप से शुरू और सक्षम किया है।
वे भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईसीआरए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और भारत में यूएस एजुकेशनल फाउंडेशन के बोर्ड में हैं। वे प्रबंधन शिक्षा और कॉर्पोरेट प्रबंधन दोनों से जुड़े नीतिगत मुद्दों के भी प्रमुख सदस्य रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया विलय समिति और प्रबंधन शिक्षा के लिए नीति-परिप्रेक्ष्य समिति की उल्लेखनीय सदस्यताएँ हैं। उनकी विशिष्ट सेवाओं को देश द्वारा स्वीकार किया गया जब भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2003 में उन्हें प्रतिष्ठित ‘पद्मश्री’ से सम्मानित किया।
पटना के वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्र का कहना है कि “बिहार में जातियां और उपजातियां राजनीति में वोट के लिए निर्णायक रही हैं। सरकारी सेवा में आजादी के पहले और बाद में कायस्थ जो कभी राजाओं और जमींदारों के यहां मुंशी होते तथा बंगाली (बिहार बंगाल से ही अलग हुआ रहता) की संख्या सबसे ज्यादा रही। भूमिहार और राजपूत जमीन से जुड़े रहे, दोनों को शोषक वर्ग (एक्सप्लोइटर्स क्लास) ही मानते हैं। जबकि भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में ये लोग काफी आगे आते रहे। इसका वजह यह था और आज भी है इनका शासन करने का अन्तर्निहित प्रकृति।”

मिश्र आगे कहते हैं कि “वकालत में मुंशी जी मिलेंगे, जिन्हें पहले मुख्तार कहते थे, इनकी अगली पीढ़ी के अधिवक्ता और बैरिस्टर बना। पटना उच्च न्यायालय में एडवोकेट्स एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष राजेंद्र बाबू बने जो राष्ट्रपति हुए। आजादी के लड़ाई में बृजकिशोर बाबू जैसे वकील ने मोहन दास करमचंद गांधी की पैरवी की। उच्चतम न्यायालय में हाल तक नवीन संज्ञा, चंद्रमौली प्रसाद गेट, जो कायस्थ थे, कुल्हाड़ियां वाले के बी न सिंह पटना और मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हुए। परिस्थितियों के कारण 1990 में लालू प्रसाद और नीतीश के काल में पिछड़ी जाति के वकील जज बने, दलित भी नियुक्त किए गए और भूमिहार तथा राजपूत की एकाधिकार खत्म हो रही है। ब्राह्मण तो उपेक्षित ही रहे।”
बहरहाल, 11वें विधानसभा के कालखंड में जब प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व के पत्र-पत्रिकाओं के पन्नों पर और टीवी के पर्दों पर ऐतिहासिक चारा घोटाला काण्ड प्रकाशित होने लगा और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर का रास्ता इस कदर दिखाया गया कि फिर कभी वापस नहीं आये, लालू यादव 4 अप्रैल, 1995 से 25 जुलाई, 1997 तक दो साल 112 दिन रहने के बाद अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार के सचिवालय में प्रवेश दिलाये। श्रीमती राबड़ी देवी 25 जुलाई, 1997 से 11 फरबरी, 1999 तक राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रदेश का कमान संभाली।
उन दिनों ये.आर. किदवई बिहार के लात साहब थे। यह कालखंड 11 वें विधानसभा का था। 11 फरवरी, 1999 से 9 मार्च, 1999 तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा और फिर 9 मार्च, 1999 से 2 मार्च, 2000 तक एक साल में छह दिन कम, यानी, 359 दिनों के लिए 11 वीं विधानसभा कालखंड में ही श्रीमती राबड़ी देवी पुनः मुख्यमंत्री कार्यालय में विराजमान हुई। अब तक प्रदेश के लाट साहेब सुन्दर सिंह भण्डारे आ गए थे। सुन्दर सिंह भंडारे के बाद न्यायमूर्ति एम.बी. लाल और सूरज भान प्रदेश के लाट साहब कब बने और कब गए, बिहार के लोगों को मालूम भी नहीं हो सका। तभी 23 नवम्बर, 1999 से 12 जून, 2003 के कालखंड में तीन साल 201 दिनों के लिए लाट साहब के कोठी में विराजमान हुए विनोद चंद्र पांडे। पांडे जी राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे जो 1989-1990 प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कालखंड में मंत्रिमंडल सचिव भी थे। मंत्रिमंडल सचिव के पूर्व जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के वित्त मंत्री थे, पांडे जी राजस्व सचिव थे। बाद में वे झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल बने। खैर।
2000 के कालखंड में, यानी 12 वें विधानसभा में, नीतीश कुमार समता पार्टी के तरफ से सात दिनों के लिए (3 मार्च से 10 मार्च, 2000 तक) मुख़्यमंत्री कार्यालय में आये और फिर बाहर निकल गए। विनोद चंद्र पांडे के कालखंड में ही श्रीमती राबड़ी देवी फिर एक बार मुख्यमंत्री (11 मार्च, 2000 से 6 मार्च, 2005) बनी। फिर समय आया राष्ट्रपति शासन का जो 7 मार्च, 2005 से 24 नवम्बर, 2005 तक कायम रहा। 13 वें विधानसभा के लिए चुनाव तो हुआ लेकिन सरकार नहीं बन सकी और फिर आया समय नीतीश कुमार का जो 24 नवम्बर, 2005 को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे।
बिहार में साल 1990 से 2005 तक और फिर उसके आगे प्रदेश के शाशन, प्रशासन, अर्थ, सभी क्षेत्रों में क्या दशा हुआ और क्या दुर्दशा हुआ, यह बिहार के मतदाता मुझसे अधिक जानते हैं। अगर प्रशासनिक दृष्टि से इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़े को ही देखें तो लालू-राबड़ी के 1991 से 2005 के बीच प्रदेश के चिकित्सक किस मानसिक तनाव से गुजरे, यह वे तो जानते ही हैं, प्रदेश के नेता, पत्रकार, लेखक, विश्लेषक अधिक जानते हैं। क्योंकि उसी कालखंड में अख़बारों के पन्नों पर, पत्र-पत्रियकाओं में, टीवी के पार्डन पर ‘लालू का जंगल राज’ लिखा मिलता था। वैसे, देश में लोग बाग़ कहते हैओं कि उस कालखंड में लालू यादव के बाद श्रीमती राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री थी, फिर ‘लालू का जंगल राज’ क्यों? अब ऐसे प्रश्नकर्ता को कैसे समझाया जाय कि आज़ादी के 78 साल और देश को गणतंत्र घोषित होने के 77 साल बाद भी देश में अभी महिलाओं को वह अधिकार नहीं मिला है, देश में अभी भी पैतृक सत्ता है – पुरुष प्रधान समाज है, और इतने दिनों बाद भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के लिए माथा पीटना पड़ रहा है।
लालू-राबड़ी के कालखंड में कोई भी सुरक्षित नहीं था। विधायक अजीत सरकार, विधायक देवेंद्र दुबे, चुनाव लड़ रहे छोटन शुक्ला या मंत्री बृजबिहारी प्रसाद, सभी की हत्या कर दी गई। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी मां, भतीजी और दो मेड के साथ दुष्कर्म किया गया। डीएम जी कृष्णैया की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह वह दौर था जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं थे। यहां तक कि अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। लालू यादव के साले सुभाष यादव और साधु यादव की दबंगई जगजाहिर है।
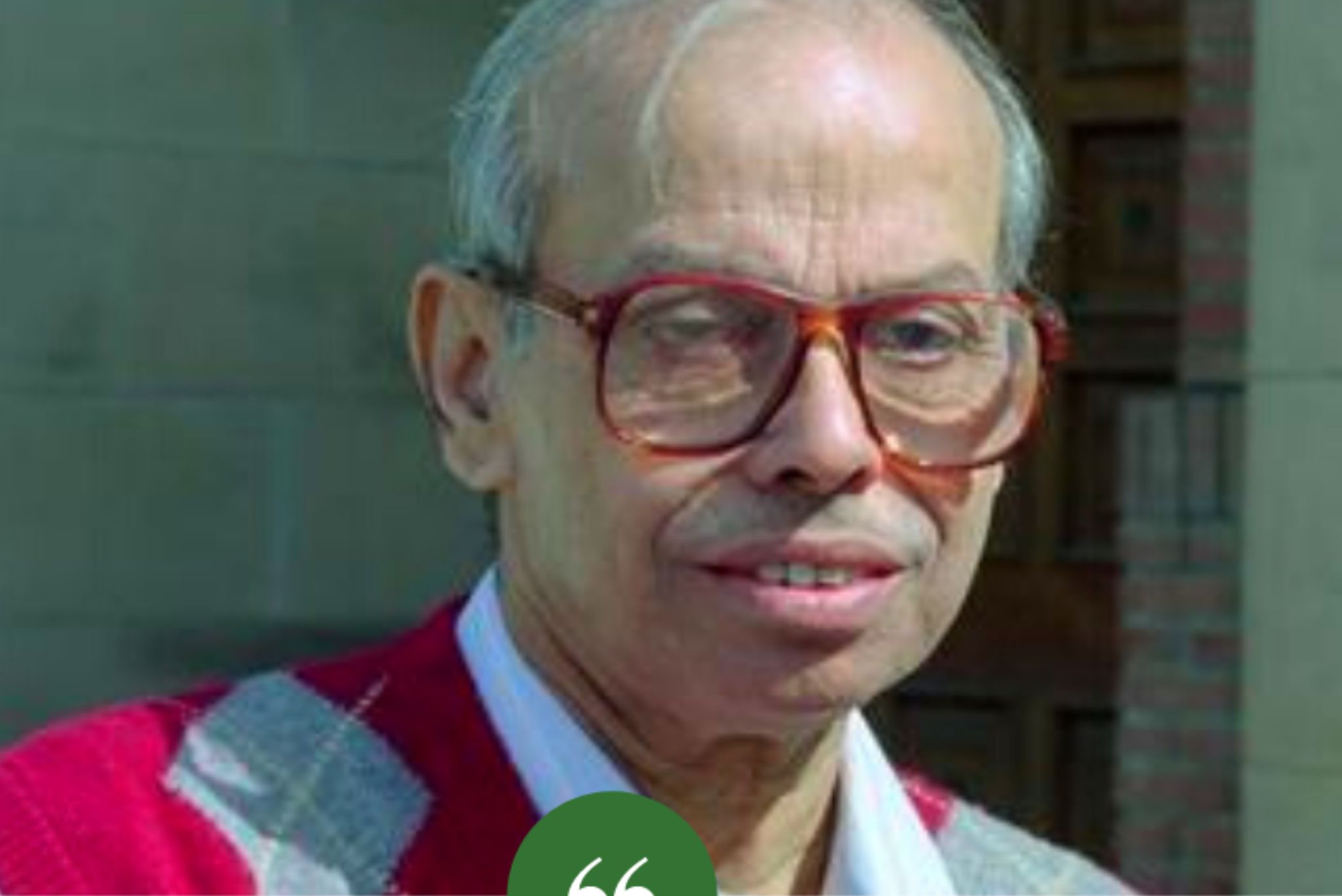
इन 15 सालों में से 8 साल तक उनकी पत्नी राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री रहीं। लेकिन उनके कार्यकाल के पीछे वे ही मास्टरमाइंड थे। इन 15 सालों में बिहार में हत्या और अपहरण एक ‘उद्योग’ बन गया। यह पैसा कमाने का सबसे पसंदीदा जरिया था। अधिकारियों, माफियाओं और राजनेताओं के बीच जो गठजोड़ बना, वह भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। यह वह दौर था जब डॉक्टर से लेकर इंजीनियर और नौकरशाह से लेकर व्यवसायी तक, उस दौर में जो भी अच्छी कमाई कर रहा था, उसे सुरक्षित रहने के लिए अपराधियों को पैसे देने पड़ते थे। लालू यादव के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब थी। यह इतनी खराब स्थिति में थी कि अगर कोई शाम 6 बजे तक घर वापस नहीं आता तो परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मच जाता था। पता नहीं कब कौन मारा जाएगा या धरती से गायब हो जाएगा। जब भी पुलिस किसी की लाश बरामद करती तो लोग अपने रिश्तेदारों या किसी और के बारे में सोचते थे। रोजगार और शिक्षा तो चर्चा का विषय भी नहीं थे।
कारोबारियों के लिए स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी बिहार में कारोबार नहीं करना चाहता था। बिहार में कई गुंडे-बदमाश नेता और ठेकेदार थे। यह एक पूरी व्यवस्था थी, जिसमें माफिया विकास कार्यों के टेंडर लेते थे। ऐसे गिरोहों के अधीन पूरी हो चुकी परियोजनाओं की स्थिति समझी जा सकती है। जब कोई अपराधी नेता बन जाता है और अपने जैसे सौ लोगों को पालता-पोसता है, तो यह ‘उद्योग’ बिना किसी डर के तेजी से बढ़ता है। 2003 में 3652 हत्याएं और 1956 अपहरण हुए। 2004 में 3861 लोगों की हत्या हुई, 1297 डकैती के मामले दर्ज किए गए, 9199 दंगे दर्ज किए गए और 2566 अपहरण के मामले दर्ज किए गए और 8189 दंगे हुए। हर साल राज्य में करीब 10,000 दंगे होते हैं। 2004 में बिहार में 3948 लोगों की हत्या हुई। इसके अलावा, जबरन वसूली के लिए 411 अपहरण और 1390 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। उनके कार्यकाल में नक्सली हमलों में कई गुना वृद्धि हुई। 2005 में बिहार में 3471 हत्याएं दर्ज की गईं। 251 अपहरण की घटनाएं और 1147 बलात्कार की घटनाएं भी दर्ज की गईं।
आईएमए के आंकड़े के अनुसार उस कालखंड में तक़रीबन चार दर्जन से अधिक चिकित्सकों या उनके आश्रितों का अपहरण किया गया था और एक दर्जन से अधिक चिकित्सकों को फिरौती के लिए मार दिया गया था। इसमें आईएमए-बिहार और बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के चिकित्सक थे। पिछले वर्ष नवम्बर के आईएमए के एक आंकड़े के अनुसार (2017 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार) देश में 75 फीसदी से अधिक चिकित्सकों ने अपने-अपने कार्य स्थल पर हिंसा का अनुभव किया, जबकि लगभग 63% हिंसा के डर के बिना मरीजों को देखने में असमर्थ थे। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि लगभग 70% डॉक्टरों को काम के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ा।
क्रमशः …..















