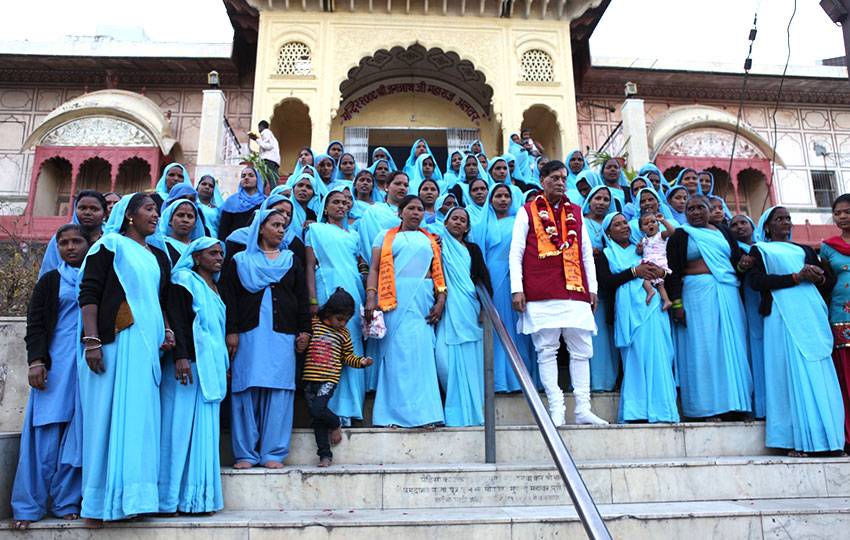
आज भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकारें “स्वच्छ भारत अभियान” के नाम का “ताल” चाहे जितना “ठोक” ले, इस अभियान के नाम पर चाहे जितना “कबड्डी खेल” ले, अभियान की सफलता का चाहे जितना “चौका” “छक्का” फेंके; सच तो यही है कि आज से पचास साल पूर्व अगर “सुलभ शौचालय” दसकों से चली आ रही एक घृणित और अमानवीय कार्य के प्रति देशव्यापी आन्दोलन नहीं चलाया होता, अपनी सोच को जमीन पर क्रियान्वित नहीं किया होता, तो आज भी समाज का एक विशाल समुदाय, एक विशाल मतदादातों का समूह, जो राजनीतिक बाज़ार में सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह, उसकी पत्नियाँ, उसके बेटे-बेटियाँ, बहुएँ अपने-अपने सर पर भारतीय सम्भ्रान्तों का “मल-मूत्र-टट्टी-पैखाना उठाते रहता” और दरवाजे से दूर रात की बची रोटियाँ लोगबाग फेंककर उसे देते रहते। पढ़ने-पढ़ाने शिक्षित होने, रोजगार-नौकरी पाने की बात तो वह अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था – न जीवित और न ही मरणोपरान्त।
यदि देखा जाय तो आज गाँधी के विचार और उनके सपने राजनीतिक बाजार में बिक रहे हैं, खुलेआम। जबकि सच तो यह है कि कोई भी शाशन, व्यवस्था या सरकार कभी भी भंगी-समाज का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक उत्थान चाहती ही नहीं थी। और अगर ऐसा नहीं था तो आज़ादी के बाद भी सरकार इस विशाल समुदाय को विकास की मुख्यधारा में क्यों जोड़ी – पूर्णतः।
वैसे सरकार और व्यवस्था के अनुसार भारतीय संविधान के मद्दे नजर अस्पृश्यता, दहेज, बाल विवाह, जाति व्यवस्था और अन्य अनेक सामाजिक बुराइयों को खत्म कर दिया गया है। लेकिन धरातल पर ये सभी कुप्रथाएं आज भी समाज में विद्यमान है। इतना ही नहीं, मानव मल-मूत्र की सफाई की प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बना है, लेकिन व्यवहार में सरकारी और सामाजिक उदासीनता के कारण वह प्रभावी नहीं हो पाया कोई पचास के दसक और उसके बाद भी जब तक ”सुलभ” ने सामाजिक आंदोलन नहीं चलाया, शौचालय की उपयोगिता को नहीं बताया, इन भंगी-परिवारों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास नहीं किया ।
कल तक जो लोग, विशेषकर समाज व्यवस्था के संभ्रांत लोग, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, कॉर्पोरेट, मंत्री, अधिकारी और न जाने कौन-कौन, अपने “खाने के मेज पर शौच की बात करना मानवीयता और मनुष्यता के खिलाफ समझते थे; आज शहरों और महानगरों, यहाँ तक की कारपोरेट घरानों, सरकारी कार्यालयों में “भोजनावकाश” के समय “भोजन करते लोग मल-मूत्र के बारे में बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि सुलभ ने अपने पांच-दसक के प्रयास से न केवल गाँधी का सपना साकार किया जमीन पर, बल्कि “भारत से मैला ढोने की कुप्रथा को भी समाप्त किया।”
अब तो जो हो रहा है विभिन्न अभियानों के तहत, वह तो महज “शौचालयों का राजनीतिकरण” है और अगर ऐसा नहीं है तो १२० करोड़ की आवादी वाले देश में, ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक १४०० व्यक्तियों पर एक शौचालय है। वैसे केंद्र सरकार के लोग बाग़ यह कहते नहीं थक रहे हैं कि आगामी २०१९ तक प्रत्येक घरों में शौचालय हो जायेगा। इसके लिए तो ब्रह्माण्ड से विश्वकर्मा को ही धरती पर अवतरित होना होगा।
बहरहाल, डॉ पाठक ने लगभग अपना सारा जीवन स्वच्छता के क्षेत्र में और हाथ से मानव-मल-मूत्र उठाने की समस्या को खत्म करने की कोशिश में लगाया । उन्होंने इसी विषय पर अपनी पीएचडी की और अन्य शिक्षा संबंधी कार्य उस वक्त शुरू किए, जब उन्होंने 1970 में सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की जो बाद में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन बन गया।
जब संडेपोस्ट उनसे पूछा: “अगर सुलभ, जिसने स्वच्छता अभियान की नीव ५० वर्ष पहले डाली थी, नहीं होता तो “भारत में स्वच्छता का हश्र क्या होता?” इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा: “इस बात का उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा की अगर सुलभ नहीं होता तो देश में भंगी-मुक्ति नहीं हो पाता और आज भी उस समुदाय के लोग अपने सर पर मैला उठाते रहते।”
कुछ समाज शास्त्रियों का मानना है कि ‘खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने का पहला सर्वाधिक प्रभावकारी तरीका है सुलभ शौचालय का निर्माण जिसका आधार है दो गड्ढों वाला (टू पीट फोर फ्लश) शौचालय, जिसमें मौके पर ही बिना हाथ लगाए सफाई हो जाती है। यह किफायती है, सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जलवायु संबंधित स्थितियों के लिए उपयुक्त है। मैले की मौके पर सफाई एक नई अवधारणा है जिसे यदि वैश्विक स्तर पर स्वीकार कर लिया जाए तो वह बहुत बड़े पैमाने पर हमारी नदियों को प्रदूषण मुक्त और शहरों को साफ-सुथरा रखेगी।
उनका कहना है कि अभी तक तो हमारे पास सीवेज अपजल निस्तारण विधि रही है, जो कि मंहगी है, प्रदूषण पैदा करती है और जिसके लिए स्कैवेंजर की जरुरत होती है। सुलभ की दो गड्ढे वाली शौचालय प्रणाली इन सभी समस्याओं का निदान है और यही कारण है कि सुलभ की इस तकनीक को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। उसे निजी घरों और सार्वजनिक शौचालय परिसरों में लगाया गया है।
अकेले कानून हाथों से की जाने वाली स्कैवेंजिंग को खत्म नहीं कर सकता । राज्य-सरकारों तथा केंद्र-सरकार ने कानून बनाए हैं- स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए निधि की व्यवस्था भी की है, लेकिन यह उस स्तर तक कारगर साबित नहीं हुआ है, जितना कि होना चाहिए। सरकार ने हाथ से सफाई करने वाले स्कैवेंजरों के लिए १०० करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, लेकिन किसी भी राज्य से धन नहीं लिया क्योंकि यह जानते ही नहीं थे कि हाथों से सफाई करने वाले स्कैवेंजरों को किस तरह पुनर्वासित किया जाए।
इसलिए जब हम शौचालय की बात करते हैं, तब हम समूची सभ्यता की बात करते हैं- अर्थव्यवस्था सामाजिक मूल्य, विचारधारा, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं। सामाजिक परिवर्तन घटित होने में समय लगता है, क्योंकि वह सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शिक्षा और सामाजिक मूल्य से जुड़ा होता है। अब हमें वह प्रक्रिया शुरू करनी है। वह हमने कर ली है। हमने सामाजिक परिवर्तन की राह में लंबी दूरी तय की है, उसके लिए एक संपूर्ण स्वच्छता व्यवस्था गठित करके। (क्रमशः)
















गजब की बकवास लिखी है, pura uttar jaldi hi dunga